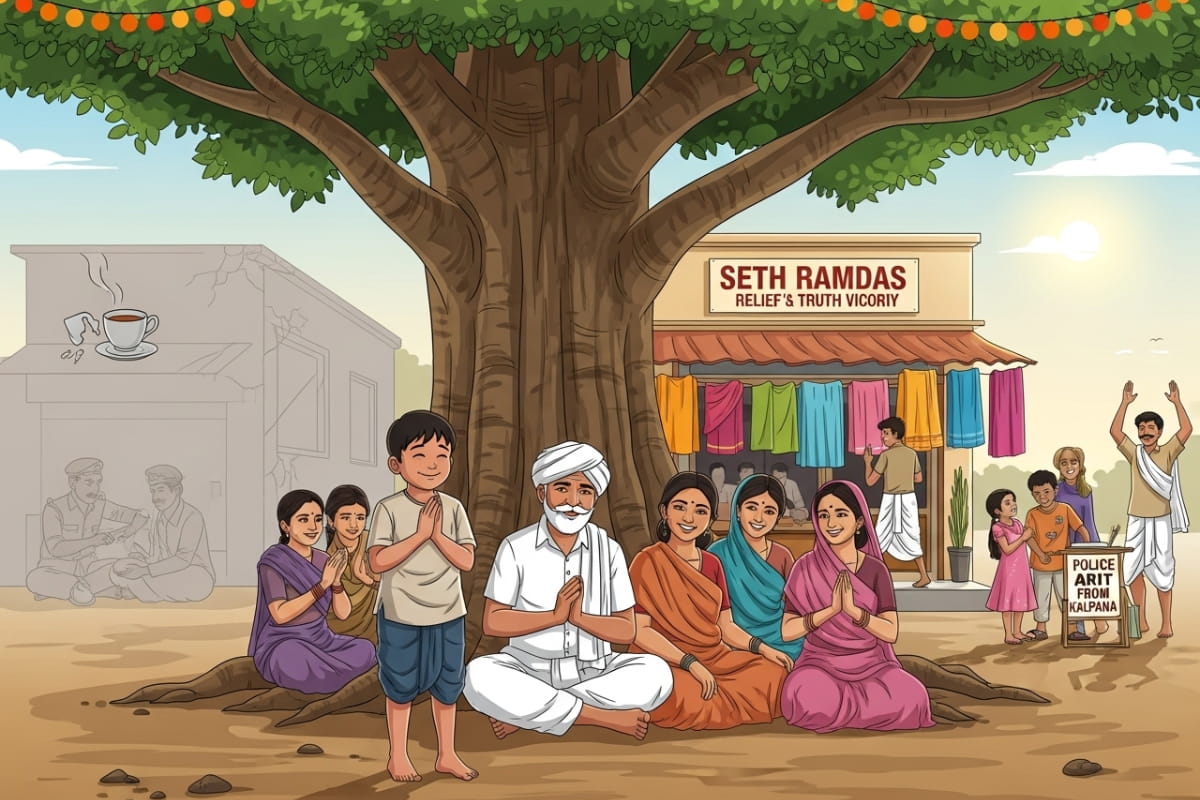वीरेंद्र को अपनी सेना भी मिल गई और जनता का आशीर्वाद भी। उसने विद्रोह छेड़ दिया। रेगिस्तान की रेत से लेकर पहाड़ की चोटियों तक “जय अमरगढ़” का नारा गूंज उठा। भैरव सिंह ने लाख कोशिश की, लेकिन जनता अब जाग चुकी थी।
आख़िरी युद्ध का दिन आया। आसमान में काले बादल थे, धरती पर खून की नदियाँ। भैरव सिंह अपने हाथी पर बैठा था, तलवार चमक रही थी। उसके सामने खड़ा था वीरेंद्र — उसकी आँखों में वही आग थी जो कभी रणधीर सिंह की आँखों में थी। दोनों के बीच युद्ध शुरू हुआ। भाले टकराए, तलवारें चमकीं, और धरती थर्रा उठी।
वीरेंद्र ने कहा — “जिस गद्दी पर तू बैठा है, वो मेरे पिता की थी। जिस जनता पर तूने जुल्म किया, उसका हक़ मैं लेकर रहूँगा।” भैरव सिंह हँसकर बोला — “राज सिंहासन खून से मिलता है, और मैंने अपना हक़ ले लिया।” वीरेंद्र दहाड़ा — “तूने हक़ नहीं छीना, तूने धोखा दिया। धोखे से पाया गया ताज हमेशा खून में डूबकर ही खत्म होता है।”
युद्ध घंटों चला। अंत में वीरेंद्र ने अपने पिता की तलवार से भैरव सिंह का सिर धड़ से अलग कर दिया। युद्धभूमि खून से लाल हो गई। जनता ने पहली बार आज़ादी की सांस ली।
वीरेंद्र सिंहासन पर बैठा, लेकिन उसकी आँखों में कोई लालच नहीं था। उसने कहा — “मैं राजा नहीं बनना चाहता, मैं तो सिर्फ़ एक सेवक हूँ। ये गद्दी जनता की है, और जनता का हर बेटा उसका रखवाला।”
अमरगढ़ फिर से खुशहाल हो उठा। खेतों में हरियाली लौटी, खदानों का सोना जनता की भलाई में लगा। लोग वीरेंद्र को भगवान मानने लगे। पर वो हमेशा कहता — “मैं भगवान नहीं, अपने पिता का बेटा हूँ… और इस धरती का सेवक।”
कभी-कभी रात को वो आकाश की ओर देखता और फुसफुसाता — “माँ, तुम्हारी कुर्बानी व्यर्थ नहीं गई। पिताजी, आपका बेटा आज अमरगढ़ का सिरमौर बन गया है।” और आसमान से जैसे आशीर्वाद की बूँदें बरस जातीं।